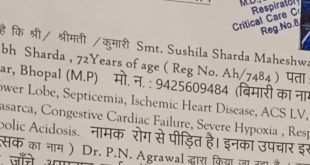*Rastrapati राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही है। 2040 में 15 करोड़ प्रकरण की संभावना*
*Rastrapati राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही है। 2040 में 15 करोड़ प्रकरण की संभावना*
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट भोपाल से राधावल्लभ शारदा के साथ होने की संभावना
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले भी सुझाव आते रहे हैं। विधि आयोग 1958 और 1978 में दो अलग-अलग संस्तुतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर इस संबंध में सुझाव और निर्देश दिए हैं।
समय की मांग है भारतीय न्यायिक सेवा, राष्ट्रपति ने दिया अहम सुझाव
भारतीय न्यायिक सेवा आज समय की मांग है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हाल में न्यायिक सुधारों की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही है। संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की युवा-शक्ति को न्यायपालिका में उसी तरह के करियर का मौका मिलना चाहिए, जैसा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के मामलों में है। उन्होंने न्यायपालिका के विशेष स्थान को रेखांकित करते हुए कहा कि अपनी विविधता का सदुपयोग करते हुए हमें ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया से विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले भी सुझाव आते रहे हैं। विधि आयोग 1958 और 1978 में दो अलग-अलग संस्तुतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। आयोग का मत था कि इससे अदालतों में लंबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण में आसानी होगी, न्यायिक-संरचना अधिक पारदर्शी तथा क्रमबद्ध हो जाएगी और उसके परिणामस्वरूप मुकदमों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों का उन पर भरोसा बढेगा। संसद की एक स्थायी समिति ने भी 2006 में इस विषय पर सुझाव दिया था। इसके अलावा इस समिति ने एक मसौदा भी तैयार किया था, किंतु वह आगे नहीं बढ़ पाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर इस संबंध में सुझाव और निर्देश दिए हैं। 1992 में आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। फिर 1993 में इस पर जरूरी पहल की जिम्मेदारी सरकार के विवेक पर छोड़ दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों के चयन के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था के निर्माण करने का सुझाव दिया, किंतु अब तक इस पर कुछ ठोस पहल नहीं की जा सकी है।
लोकशाही में उसके सभी उपांगों की विश्वसनीयता उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अदालतों के मामले में तो यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उनकी एकमात्र पूंजी होती है। जनता के बीच उनकी साख और आम लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान ही उनकी ताकत होती है। इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सजग रहने की जरूरत होती है। लंबित मुकदमों का अंबार, उनके निस्तारण में देरी तथा पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाएं न्यायपालिका की साख को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। पारदर्शिता के प्रति आग्रही समाज में गैर-जरूरी गोपनीयता कई बार अविश्वास के काल्पनिक कारणों तथा आधारों को तैयार करने की पृष्ठभूमि बनाती है। कोलेजियम व्यवस्था की गोपनीयता के कारण उस पर प्रश्न उठने लगे हैं। ऐसे में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के पक्ष में पर्याप्त आधार दिखते हैं।
न्यायपालिका की अखिल भारतीय सेवा पूरे देश के लिए एक ऐसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें हमारे समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। इसमें समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। चूंकि यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसलिए इसमें सबसे अच्छे लोगों के चयन की एक परंपरा विकसित होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां न्यायाधीशों की बहुत कमी है।
अमेरिका में जहां हर 10 लाख की आबादी पर 107 न्यायाधीश हैं, वहीं अपने देश में अभी हम इतनी आबादी पर 21 न्यायाधीशों के पद ही सृजित कर पाए हैं। अलग-अलग राज्यों में उनके चयन की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती रहती है, जिसके कारण कुल 25,246 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 19,858 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार, मुकदमों के दायर होने की वर्तमान दर के मुताबिक 2040 में कुल 15 करोड़ मुकदमे लंबित होंगे, जिनके निस्तारण के लिए 75,000 न्यायाधीशों की जरूरत होगी। विभिन्न राज्य सरकारों की मौजूदा कार्यपद्धति को देखते हुए यह संभव नहीं लगता। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से इस चुनौती से निपटना आसान हो जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में कहा गया है कि इसके द्वारा चयनित व्यक्ति जिला न्यायाधीशों के बराबर होगा। जिस तरह अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आबादी के अनुपात में पदों का सृजन होता है, उसी तरह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में होगा। आबादी तथा मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या हो जाने से मुकदमों का बोझ कम होगा।
इस समय न्यायपालिका में चयन के लिए दो पद्धतियां हैं। जिला अदालतों के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है। उच्च न्यायालयों के 25 प्रतिशत पद न्यायिक अधिकारियों की प्रोन्नति से, जबकि शेष पद अधिवक्तागण में से कोलेजियम द्वारा भरे जाते हैं। जिला अदालतों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से न्यायिक सेवा में आने वाले न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बारे में तो उनके लिए कल्पना करना भी कठिन है। इन परिस्थितियों में उनके मन में बंचना-बोध पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्रतिभाशाली छात्रों का रुझान इस सेवा की ओर कम होता जा रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रतिभावान न्यायाधीशों का ऐसा विकल्प होगा, जो इस संस्था की प्रतिष्ठा को नई उंचाई दे सकते हैं
( हरवंश दीक्षित – लेखक विधि शास्त्र के प्राध्यापक हैं)
 mahadandnews.com mahadandnews | www.mahadandnews.com
mahadandnews.com mahadandnews | www.mahadandnews.com